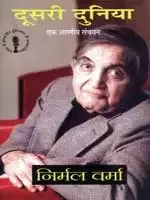|
जीवनी/आत्मकथा >> दूसरी दुनिया दूसरी दुनियानिर्मल वर्मा
|
310 पाठक हैं |
||||||
निर्मल वर्मा का आत्मीय संचयन...
doosri duniya
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
बोलना, निर्मल वर्मा के वहाँ कथन (स्टेटमेंट) नहीं है। वक्ता का जोर बावजूद इसके कि उसमें ‘सच’ और ‘झूठ’ और ‘पाप’ जैसे मूल्याविष्ट प्रत्यय बार-बार आते हैं, अपने बोले हुए की टुथ-वैल्यू पर उतना नहीं, जितना खुद को उच्चरित करने पर है....दरअसल उनके पात्र भाषा से तदात्म हस्तियाँ हैं। भाषा के जल में उठती हुई लहरें। भाषा में उत्पन्न नए अर्थ....वे साँचे हैं जो अब नहीं हैं लेकिन जिनके कभी होने का पता हमें उस भाषा से चलता है जो इन साँचों में ढली है, जो हमारे सामने है....यह भाषा अपने ‘टैक्सचर’ की पर्याप्त प्रांजलता के बावजूद अपने ‘स्ट्रक्चर’ में अत्यंत अर्थगर्भी और जटिल है लगभग एक कूट की भाँति.....
निर्मल वर्मा का हर पात्र कथा के एकान्त में एक देह है: ‘एक गुप्तचर की तरह अपने कोड (केट) में विचित्र संदेश देती हुई, अपने अतीत अपने यातनाओं के बारे में’ निर्मल वर्मा स्वयं किसी तरह की तर्कणा या परिपृच्छा से उसे पुकार कर या झिंझोड़ कर उसका एकांत भंग नहीं करते। वे इस कूटबद्ध देह (वाक्य) के लिए एक अवकाश रचते हैं अपनी कथा के माध्यम से ऐसा ‘घना सन्नाटा’ जहाँ इस देह के विचित्र संदेश ग्रहण किए जा सकें; जहाँ उसकी ‘गुप्त गवाही का गवाह’ हुआ जा सके.....उनके यहाँ मनुष्य का सत्व भाषा में रूपायित है।
निर्मल वर्मा का हर पात्र कथा के एकान्त में एक देह है: ‘एक गुप्तचर की तरह अपने कोड (केट) में विचित्र संदेश देती हुई, अपने अतीत अपने यातनाओं के बारे में’ निर्मल वर्मा स्वयं किसी तरह की तर्कणा या परिपृच्छा से उसे पुकार कर या झिंझोड़ कर उसका एकांत भंग नहीं करते। वे इस कूटबद्ध देह (वाक्य) के लिए एक अवकाश रचते हैं अपनी कथा के माध्यम से ऐसा ‘घना सन्नाटा’ जहाँ इस देह के विचित्र संदेश ग्रहण किए जा सकें; जहाँ उसकी ‘गुप्त गवाही का गवाह’ हुआ जा सके.....उनके यहाँ मनुष्य का सत्व भाषा में रूपायित है।
उत्तरी रोशनियों की ओर
दिन और रात....
कित्ता पानी ? कित्ता ? हाथ फैल जाते हैं, और नन्हें से आलिंग्न में समूचा अन्तहीन समुद्र सिमट आता है। मुद्दत पहले घर की छत पर मछलियों का खेल खेलते हुए क्या कभी सोचा था कि एक दिन सचमुच लहरें हमारे सिर पर से गुज़र जाएँगी और हम, जो अब बड़े हो गए हैं, बच्चों से डरते, ठिठुरते हुए डेक पर बैठे रहेंगे ?
या लेटे रहेंगे, कम्बलों में सिकुड़े हुए बंडलों-से-लंच की घंटी बजेगी तो भी, ‘डिनर’ की पुकार होगी तो भी ! बिना हिले-डुले, भूखे-प्यासे तपस्वियों से, अधसोए, अधजागे...
रात और दिन..
दो दिन तक समुद्र-पक्षी बराबर हमारे जहाज़ के पीछे उड़ते रहे, धूप और आँधी में, दिन-रात। जब जहाज़ के ‘किचन’ से बावर्ची पुरानी बासी रोटी के टुकड़े, फलों के छिलके या बची-खुची गोश्त की तरकारी बाहर फेंकता, तो वे उन पर उतावले-से होकर टूट पड़ते, समुद्र में गोते लगाते हुए उन्हें निगल लेते और फिर उड़ने लगते, उस घड़ी की आशा में जब बारह या तेरह घंटे बाद बावर्ची फिर अपना सिर ‘किचन’ की खिड़की से बाहर निकालेगा।
किसने कहा था कभी समुद्र-पक्षी के ‘रोमैंटिक’ सौन्दर्य के बारे में ? छह दिन का सागर-पथ है। कोपनहेगन से आइसलैंड तक। हर दिन को गिनना पड़ता है, समय का हिसाब रखने के लिए। और समय है जिसने अपने को दिन और रात के पहियों से मुक्त करके फैला दिया है, समुद्र की अबाध नीलिमा पर। लम्बे होते हुए दिन, सफ़ेद रातों-तले चीख़ती लहरें, पानी के बीच धरती पाने की बिलखती प्यास...
उदासी, चक्कर, थकान, इन सबसे मुठभेड़ बाद में हुई। पहले दिन सबके चेहरे पर ताज़गी, उल्लास और ललक, भोजन के प्रति उत्साह आधे पढ़े हुए उपन्यासों को ख़त्म करने की उमंग, नए मित्र बनाने का जोश-सबकुछ था। डेक की कुरसियाँ भरी रहतीं लड़कियों के बालों पर बँधे लाल, नीले हरे स्कार्फ़ हवा में उड़ते रहते, जहाज़ के कामों में प्रमियों के जोड़े समुद्र पर तिरते हुए सपनों में खोए रहते। जब कभी मौसम अच्छा होता, सब अपने-अपने कम्बलों में लिपटे हुए धूप सेंकने बैठे जाते। विभिन्न देशों के यात्री वहाँ जमा थे-स्विस, जर्मन स्वीड, डेन और अकेला एक भारतीय ! डेक के ऊपर ‘बार’ थी, फर्स्ट क्लास के सामने। अकसर रात्रि के भोजन के बाद जब डेक पर हवा तेज़ हो जाती और कम्बलों के बावजूद दाँत कटकटाने लगते, यात्रियों के छोटे-छोटे गुच्छे ‘बार’ में जा बैठते। बन्द खिड़कियों के परे समुद्र की अधीर, बेचैन चीखडें गूँजती रहतीं, मानो किसी बनैले जन्तु के पिंजड़े में बन्द कर दिया हो और वह हाँफता, बदहवास-सा होकर बाहर निकल आने के लिए छटपटा रहा हो ! चिड़ियाघर में बन्द क्या कभी सिंह को देखा है, उसकी क्षुब्ध, असहाय विक्षिप्त घुटन को ?
किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लमहों के लिए डेनिश बीयर या फ्रेंच कोन्याक पीते हुए हम भूल जाते कि हम असीम अँधेरे के एक छोटे-से टुकड़े पर तिर रहे हैं, कि हमारे नीचे एक नीली, रहस्यमय जादुई दुनिया बसी है, हमारे संग-संग रेंग रही है-क्षुब्ध, अशान्त और निस्तब्ध। इस दुनिया का आभास उसी समय होता जब कोई अल्लहड़ सी लहर पूरी निर्ममता से हमारे जहाज़ को धकेल देती और अचानक हमारे सामने मेज़ पर रखा बीयर का गिलास लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ता, और ‘बार’ में हर मेज़ पर अपने-अपने गिलासों को बचाने की बचकानी-सी भगदड़ मच जाती।
किन्तु समुद्र का यह नशा और उल्लास ज्यादा दिनों तक नहीं टिका रह सका। उत्तरी सागर के खुले, नग्न विस्तार में पहुँचते ही हमारे जहाज़ को अचानक प्रगैतिहासिक काल की बनैली, आदिम लहरों ने लपेट लिया। जान पड़ता था जैसे कोई अदृश्य दानव हमारे ‘गुलफॉस’ को एक नन्हें-से खिलौने की मानिन्द ऊपर-नीचे उछाल रहा हो ! डेक पर दो क़दम चलते हुए लगता था, जैसे हम एक छोटे से भूकम्प के भीतर से गुजर रहे हैं। जहाज़ अब ऊपर-नीचे न डोलता हुआ दाएँ-बाएँ हिचकोले खा रहा था। डेक पर पानी के चहबच्चे लग जाते थे और अब वहाँ बैठना ख़तरे से खाली नहीं था। जहाज के बीचोंबीच एक चौड़ा-सा चबूतरा था जो अपेक्षाकृत अधिक सूखा और सुरक्षित रहता था। डेक से खदेड़े जाने के बाद हमने बचाव का दूसरा मोर्चा यहीं पर गाड़ लिया था।
इस बीच कई परिचित मित्रों से धीरे-धीरे साथ छूटता गया। पहले दिन के जाने-पहचाने साथी अब बहुत कम डेक या भोजन-कक्ष में दिखाई देते थे और हम मन-ही-मन अनुमान लगा लेते थे कि वे ‘मृत्यु-शैया’ (मज़ाक में हमने ‘सी-सिकनेस’ को मृत्यु शैया की संज्ञा दे रखी थी) के शिकार हो गए हैं। ऐसा भी होता था कि किसी शाम ‘बार’ में हम किसी हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति से हँस-खुलकर गपशप कर रहे होते और दूसरे दिन वह सज्जन ऐसे ग़ायब हो जाते कि अगले चौबीस घंटों तक उनके दर्शन ही न होते। दोबारा मिलने पर उनका पीला, जर्द़ चेहरा देखते ही हम भाँप जाते कि वह बेचारे ‘तहख़ाने’ से वापस लौटे हैं।
तहख़ाना....यह नाम हमने अपने सेकेण्ड क्लास के सामूहिक केबिन को दे रखा था। हमारे लिए अलग-अलग केबिन नहीं थे, सब मिलजुलकर एक संग बैरकनुमा कमरे में सोते थे। एक बिस्तर के ऊपर दूसरा बिस्तर लगा था, बीच में सब लोगों का सामान और ईर्द-गिर्द बहुत ही मद्धिम बत्तियाँ, जैसे ‘फ़ाइटिंग-लाइन’ के पीछे कोई छोटा-सा अस्पताल हो ! इस अँधेरे, लम्बे सीलन-भरे ‘तहख़ाने’ में घुसते ही सिर चकराने लगता था-इससे छुटकारा पाने के लिए ही हम रात-दिन डेक पर डटे रहते थे, जिसे हमने ‘फ़ाइटिंग-लाइन’ का नाम दे रखा था।
लीथ की बन्दरगाह पहुँचने से पहले जहाज़ के यात्री खुद-ब-खुद तीन वर्गों में बँट चुके थे :
1. वे यात्री जिनके लिए समुद्र का होना-न-होना बराबर था। वे अकसर आराम से अपने-अपने बिस्तरों पर सोते रहते और जब ऊब जाते तो ‘बार’ में बैठकर बीयर पीते, आइलैंड का नक्शा देखते या ‘राइटिंग-टेबल’ पर चिट्ठियाँ लिखते। वे सुबह शाम यथासमय (या समय से पहले ही) ‘लंच’ और ‘डिनर’ लेने ‘डाइनिंग रूम’ जाते थे और मुस्कराते हुए तुष्ट भाव से वापस लौटते थे। हम सब उन्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे-इसके अलावा शायद हम कुछ कर भी नहीं सकते थे।
2. डेकवासी, जो चारों ओर शत्रुओं से घिरे थे। केबिन में जाते ही जिनका सिर चकराने लगता था, भोजन-कक्ष में भोजन को देखते ही मितली आने लगती थी और ‘बार’ में बैठकर मद्य-पदार्थों के सेवन के प्रति जिनके मन में गहरी सात्त्विक निरासक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। मृत्यु शैया से अपने को मुक्त रखने के लिए जिन्होंने डेक का सहारा पकड़ रखा था। रात-दिन कड़कड़ाती सरदी में ठिठुरते अपने-अपने स्लीपिंग बैग या कम्बलों में साँस लेती गठरियों से डेक के चबूतरे पर पड़े रहते थे-‘डिफ़ेन्स-लाइन’ के सिपाही। मैं इसी मण्डली के संग आख़िर तक घिसटता रहा।
3. और अन्त में मृत्यु-शैयावासी, जो डेक के कष्टों से घबराकर अपने गरम बिस्तरों पर लेटने का मोह सँवरण न कर सके और फिर वहीं के हो रहे। तहख़ाने के बिस्तरों पर उन्हें लेटे देखकर अकसर युद्ध में घायल सैनिकों का स्मरण हो आता, जो डेक की ‘डिफ़ेन्स-लाइन’ पर क्षत-विक्षत होने के कारण जहाज़ के डॉक्टर द्वारा यहाँ भेज दिए गए हों।
तीसरे दिन सुबह बदली और कुहरे के परदे पर ज़मीन की धुँधली-सी रूपरेखा दृष्टिगोचर हुई और गो हम बहुत पस्त और थके थे, लीथ बन्दरगाह का नाम सुनते ही डूबे और टूटे हौसलों को वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमारे जहाज़ को यहाँ पाँच-सात घंटे विश्राम लेना था और इस दौरान कोई भी जहाज़ पर रहने के लिए उत्सुक नहीं था। कुछ घड़ियों के लिए हम अँधेरे तहख़ाने, डेक की सरदी और जहाज़-सम्बन्धी हर चीज से छुटकारा पाने के लिए उतावले से हो उठे थे।
ज़मीन, दुकानें लोगों की परिचित आवाज़ें और पुराने गिरजे-लगा, जैसे हम एक लम्बी मुद्दत के बाद सभ्यता की दुनिया में वापस लौट आए हैं। यद्यपि हम जहाज़ से उतरकर ठोस धरती पर चलने लगे थे, हमें देर तक यही महसूस होता रहा जैसे हम शराबियों की मानिन्द किसी डोलती, डगमगाती चीज़ पर चल रहे हों। समुद्र अब भी हमारे संग था।
मन में पहले से यह भ्रम था-हालाँकि इस भ्रम का कोई विशेष आधार रहा हो, याद नहीं आता-कि बन्दरगाह से एडिनबोरो जाने में काफी देर लगेगी, किन्तु जब बस ने सिर्फ आधा घंटे में हमें शहर के बीचोबीच लाकर छोड़ दिया तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ और कुछ-कुछ निराशा भी। सबसे पहले चाय पी, चाय और टोस्ट-और तब पहली बार पूरी वास्तविकता से एहसास हुआ कि हम इंग्लैंड में हैं....इंग्लैंड न सही, स्कॉटलैंड में, किन्तु हर चीज़ बार-बार लन्दन के बीते दिनों का स्मरण करा जाती थी। डबलडेकर लाल बसें, एल और ड्राफ्ट के बीयर-घर, घरों के दरवाजे के सामने रखी दूध की बोतलें, ‘गार्डियन’ और ‘टाइम्स’ ‘प्लेयर्स प्लीज’ के विज्ञापन, हैम्बर्गर और हॉट डॉग और पेलीकन सीरीज़ की पुस्तकें, जिन्हें देखे अरसा गुज़र चुका था....
और कुहरा !
किन्तु रफ़्ता-रफ़्ता कुहरा उठने लगा था और हम खुलती, फीकी धूप की हलकी खुमारी में भीड़ के संग-संग घिसटते जा रहे थे। पहली बार पूरी शिद्दत से महसूस हुआ कि धरती, महज ठोस धरती पर चलने का भी अपना अलग सुख है। वह पैरों के नीचे काँपेगी नहीं, हिले डुलेगी नहीं, यह ख़याल मन को अजीब सान्त्वना-सी देता है। यदि हमें उस समय कोई यह कहता कि हम जिन्दगी-भर धरती पर ही चलते रहे थे तो हमें कुछ वैसा ही विस्मय होता जैसा मोलियर के ‘जैण्टिलमैन’ को यह जानकर हुआ था कि वह जीवन-भर गद्य में बातचीत करता रहा है।
ऊँचा-नीचा शहर एडिनबोरो, प्रिन्सेज़ स्ट्रीट पर चलते हुए आम स्कॉटिश लोग, पहाड़ी लोगों-से सहज और खुशमिज़ाज। लगता है, अँगरेज़ों की अभिजात औपचारिकता इन्हें नहीं छू गई है। सड़क के बीचोबीच ठठाकर हँसते हैं और अचानक याद हो आती है रॉबर्ट बर्न्स की। प्रिन्सेज़ स्ट्रीट के सामने ही एक छोटे-से बाग़ में बर्न्स का स्मारक है और उनकी मूर्ति के सामने स्मरण हो आते हैं मुद्दत पहले पढ़े उनके गीत, उनकी कविताएँ। कितना-कुछ जो हम स्कॉट जाति के बारे में जानते-बूझते हैं : जीने और मरने की भूखी हठीली चाह, हर अन्याय के विरुद्ध सुलगता विद्रोह, एक खुरदरी उच्छृंखल-सी अराजकता, गरीबी और गर्व, दूर पहाड़ियों की पुकार और शहरी पबों की पियक्कड़ चीखें-यह सब, और इसके अलावा बहुत-कुछ भी बर्न्स के गीतों से निकलकर हमारे संग-संग चलता है, एडिनबोरो की गलियों में।
शायद यह है-और ऐसा मैं सोचता हूँ, कि हमयात्री किसी भी जगह पहली बार नहीं जाते; हम सिर्फ लौट-लौट आते हैं उन्हीं स्थानों को फिर से देखने के लिए, जिसे कभी, किसी अनजाने क्षण में हमने अपने घर के कमरे में खोज लिया था। क्या यह कभी सम्भव कि हम ओसलो में घूमते रहें और अचानक गली के नुक्कड़ पर इब्सन के किसी पात्र से भेंट न हो जाए ! या पहली बार आइफल-टॉवर के सामने फैली पेरिस की छतों को देखकर हमें ‘अपने’ पेरिस की याद न हो आए जिसे हमने बाल्ज़क के उपन्यासों और रजिस्ताँ की कविताओं से चुराकर ख़ास अपनी निजी अल्बम में चिपका लिया था।
ये ख़याल बादलों की तरह बह आते हैं, स्कॉटमेमोरियल की पहाड़ी पर, जिसकी ढलान पर हम लेटे हैं। थोर्गियेर ने कुछ फोटो लिए हैं। हलकी-हलकी रुई में भरी आवाज़ें। सामने फैला है एडिनबोरो और उसके परे मेघाच्छन्न आकाश। फ़ोर्ट की ऊँची बुर्जियों पर परिन्दों का झुण्ड उड़ा जाता है। नीचे खड़े हैं बुझी-बुझी मैली धूप में शहर के मकान, कोयले और गर्द में सनी नंगी दीवारें, ऊँची-नीची छतें, चिमनियाँ, बरामदों में सूखते, हवा में फड़फड़ाते कपड़े। शहर वही है किन्तु पहाड़ी की चोटी से देखने पर बिलकुल बदल गया है, जैसे हम उसकी फ़ोटो का ‘नेगेटिव’ देख रहे हों !
किन्तु आँखें शहर की चिमनियों के परे फिसल जाती हैं-उस ओर जहाँ धरती का आँचल भीग रहा है नीली स्याही में। एक गीला बैंगनी रंग, फीकी, धूप में घुलता, फैलता। उत्तर की ओर जहाँ एक अदृश्य बिन्दु पर आइसलैंड टिका है-नीली चट्टानें जहाँ मोम-सी बनकर धूप में पिघल रही हैं और बादल हैं, जो थिएटर के परदों से हवा में टँगे हैं, जिन्हें हमारा जहाज़ एक-एक करके उठाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा।
हम धूप में ऊँघने लगे हैं। हवा चलती है और अजीब कोमल-सी सरसराहट होती है कानों के पास। घास तितलियाँ या महज़ हवा। थोर्गियेर दूरबीन से बन्दरगाह की ओर देख रहे हैं। सोते हुए भी मुझे लहरों का स्वर सुनाई देता है...जैसे कोई रो रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं है-सिर्फ़ हवा में सरसराती घास है और ऊपर बादल हैं और समुद्र बहुत दूर है...अचानक थोर्गियार मेरा कन्धा हिलाते हैं, ‘‘देखो...उस तरफ़’’,-वह उँगली से इशारा करते हैं और दूरबीन मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं। एक नन्हा-सा सफ़ेद धब्बा दूरबीन के शीशे पर सिमट आया है-गुलफ़ॉस ! हमारा जहाज़। दूर से वह कितना अरक्षित और असहाय-सा दिखाई देता है !
‘‘अब हमें चलना चाहिए’’, थोर्गियेर ने जम्हाई लेते हुए कहा। सोने की जबरदस्त इच्छा होती है, घास पर भूल जाने की इच्छा होती है कि हमें फिर डेक की ‘डिफेन्स-लाइन’ में जाना होगा लेकिन हम नीचे उतरते जाते हैं, दोपहर की लम्बी छायाओं के संग...बीच यात्रा में मुहब्बत से बचना चाहिए,’’ एक पुरानी चीनी कविता की पंक्ति याद आती है।
समय कम और सीमित है। शाम को चार बजे तक जहाज़ पर पहुँच जाना होगा-इतना समय नहीं कि जहाज़ पर भोजन करने के बाद वापस शहर लौटा जा सके। हम चाय पीकर ही सन्तुष्ट हो गए हैं। ‘फ़ोर्ट’ और ‘आर्ट गैलरी’ के बीच चुनाव करना ही होगा, दोनों को देखने का समय नहीं है। निर्णय करने में ज्यादा ऊहापोह नहीं करनी पड़ी। हमारे पाँव एडिनबोरो आर्ट गैलरी के चौड़े दरवाज़ो की तरफ बढ़ जाते हैं।
कितने कम याद रह पाते हैं चित्र, दीवार पर टँगे फ्रेमों में बन्द खून और पसीने में लिथड़े स्वप्न ! और हम हैं कि हर कदम पर सदियों को पार करते जातें हैं। संग रह जाता है केवल एक आभास-रंगों और आकृतियों से उत्पन्न हुई किन्तु उससे अलग एक स्मृति। शून्यता को काटती एक उड़ान, एक चीख़। बन्द सदियों की कुछ चाभियाँ, जिन्हें हम अपने संग ले आते हैं और बाद में खोलते हैं; अकेले में, अपने ही अकेलेपन को।
जब कभी एडिनबोरो की ‘आर्ट गैलरी’ के बारे में सोचता हूँ आँखों के सामने घूम जाते हैं तितियान के चित्र...लगता है, जैसे मानव-आत्मा अपने सब बन्धनों को तोड़कर सुनहरे असीम आलोक के ज्वलन्त रंगों में फैल गई है। तितियान के देवदूत असीम दूरियाँ लाँघते हुए एक ऐसे मांसल आनन्द को खींच लाते हैं जिसमें रहस्यमय अथवा अशरीरी कुछ भी नहीं है, धरती के ऊपर उड़ते हुए भी जो धरती की गन्ध और आत्मीयता को नहीं छोड़ पाते और बरबस मुझे बैरन्सन के शब्द याद हो आते हैं : ‘पुनर्जागर की सच्ची पवित्र सन्तानें, जिन्दगी के भय और ओछेपन से सर्वथा मुक्त।’ गैलरी में मेरे प्रिय चित्रकारों-रैम्ब्राँ हालास और स्टील के भी चित्र हैं, किन्तु इतने कम कि भूख नहीं मिटा पाते। सिर्फ़ एक एलग्रेको। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे उस समय हुआ जब अचानक गैलरी के एक अलग छोटे-से कक्ष में सिर्फ़ पूसाँ के चित्र दिखाई दिए-‘सेवेन सेक्रामेंट्स’ का पूरा सेट। नि:सन्देह कोई भी गैलरी फ्रेंच कलाकार की इन अद्वितीय अमर कृतियों पर गर्व कर सकती है। दीवार के एक कोने में बैलिनी के वे उद्गार उद्घृत किए गए हैं जो उन्होंने ‘सेवन सेक्रामेंट्स’ को पहले-पहल देखकर प्रकट किए थे। काश, मैं उन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख पाता।
उस रात पहली बार जहाज़ के विभिन्न वर्ग आपस में घुल मिल गए और हम देर तक ‘बार’ में बैठकर बीयर पीते रहे...बिना किसी डर या आशंका के-मानो हम प्राग के ही किसी ‘पब’ में बैठे हों। समुद्र पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक स्थिर था, किन्तु यह स्थिरता ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, यह हम जानते थे। शायद इसी कारण अनेक यात्री ‘मृत्यु-शैया’ पर जाने से पहले मुक्ति के इन चन्द लमहों को खुले और अकुण्ठित मन से जी लेना चाहते थे।
लीथ छोड़ने के बाद डेक पर अनेक चेहरे दिखाई देने लगे हैं। इंग्लैंड से अनेक नए यात्री जहाज़ पर आए हैं, केवल अँगरेज़ ही नहीं, विभिन्न देशों के लोग। ‘बार’ की मेज पर दो स्विस लड़कियों से परिचय हुआ। उन्हें केवल यह चिन्ता सता रही थी कि आइसलैंड में अच्छा दूध मिलेगा या नहीं, ‘‘दूध नहीं मिला, तो ज्यादा दिन मैं नहीं रह सकूँगी।’’
‘‘दूध के बारे में मुझे नहीं मालूम लेकिन दुर्भाग्यवश बीयर पर पाबन्दी है,’’ मैंने कहा।
बीयर से उन्हें ख़ास लगाव नहीं था, अतः इस समाचार से उन्हें कोई विशेष दुख नहीं हुआ। बाद में पता चला उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है (‘क्या हमसे ज्यादा खराब ?’ मैंने मन-ही-मन सोचा) और वे ‘हिचहाइकिंग’ द्वारा ही आइसलैंड का भ्रमण करेंगी। उस रात के बाद हमने उन्हें आइसलैंड पहुँचने तक नहीं देखा..टॉमस मान के सेनेटोरियम के मरीज़ों की भाँति इस जहाज़ पर जाने-पहचाने लोग अचानक ग़ायब हो जाते हैं और फिर उनके बारे में बातचीत करना ‘बैड-टेस्ट’ माना जाता है।
लीथ की बन्दरगाह से पुरातत्त्वशास्त्र और भूगर्भशास्त्र के अनेक अँगरेज़ छात्र-छात्राएँ जहाज़ पर दिखाई देते हैं। उनका अपना एक अलग झुण्ड है और वे हमेशा एक संग घूमते हैं। किन्तु हमारे सबसे आत्मीय और दिलचस्प मित्र कुछ ‘पेसिफ़िस्ट’ युवक-युवतियाँ हैं जो आइसलैंड में लूले-लँगड़े बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने बातचीत करते हुए मुझे बताया कि यद्यपि वे एक ही संस्था के सदस्य हैं, उनमें से हर व्यक्ति को हर समस्या पर अपने स्वाधीन विचार रखने का अधिकार है। उनमें से कुछ लोग आणविक-निःशस्त्रीकरण कमेटी (अध्यक्ष : बर्ट्रेण्ड रसेल) के समर्थक हैं। एक बुद्धिजीवी से दिखनेवाले युवक ने जिनकी लम्बी ऊबड़-खाबड़ दाढ़ी है और जो हमेशा नीली जीन्स पहने रहते हैं जिनकी जेबों में किताबें भरी रहती हैं..‘बीटनिक कवि ?’ मैं सोचता हूँ), मुझे देखते ही तपाक से हाथ मिलाया है, ‘‘मैंने आपको कहीं देखा है-आप एल्डर मास्टन-मार्च में तो नहीं थे ?’’
‘‘नहीं, उन दिनों मैं इंग्लैंड में नहीं था-लेकिन शायद आपने मुझे ट्रिफ़ाल्गर स्क्वॉयर में देखा होगा, कभी-कभी मैं वहाँ जाया करता था।’’ काफ़ी देर तक हम लन्दन के बारे में बातचीत करते रहे। वह भी मेरी ही तरह ‘डेकवासी’ थे। अकसर बहसों के दौरान (वह एकतरफा नि:शस्त्रीकरण के समर्थक थे) मैं चुपचाप उनके तर्क सुना करता था।
बीच के इन दिनों में देर रात तक डेक पर लम्बी और कभी-कभी उत्तेजनापूर्ण बहसें हुआ करती थीं...लगभग सभी ‘डेक-वासी’ इनमें भाग लेते थे। एकतरफ़ा निःशस्त्रीकरण (जो सबसे ज्यादा ‘जलता प्रश्न’ था) से लेकर आइख़मैन के मुक़दमे तक...न प्रश्नों की कमी थी, न समय का अभाव। हमें काफ़ी ऊँचे स्वर में बोलना पड़ता था ताकि हमारी आवाज़ लहरों से ऊपर उठ सके।
हमारा जहाज़ अटलाण्टिक सागर के बीच आ चुका था। जितना ही अधिक वह उत्तर की ओर सरकता जाता था, रातें ज्यादा सफ़ेद होती जाती थीं। एक असीम उजाला। रात और दिन की सीमा-रेखा दिन-पर-दिन धुँधली होती जा रही थी। अकसर हम आधी रात तक अपने-अपने स्लीपिंग बेड में लिपटे डेक पर लेटे रहा करते थे। ‘बार’ की बत्ती बुझ जाती थी, फ़र्स्ट क्लास के केबिन अँधेरे में डूब जाते थे और चारों ओर एक घना, गहरा सन्नाटा घिर आता था-सिर्फ़ लहरें थीं जो कभी चुप नहीं होती थीं किन्तु अब हम उनकी ओर से निरासक्त हो चले थे। हम लेटे रहते, और धीरे-धीरे तारों से आकाश भरने लगता। जुलाई का नीरव उजला आकाश। आकाश और बहुत पुराना अतीत। हर एक की अलग स्मृतियाँ। और हम डेक पर लेटे हुए एक दूसरे की साँस सुनते रहते....नींद नहीं आती थी। तब अचानक कोई धीमे, बहुत धीमे स्वर में गाने लगता था। कोई जर्मन फ़ेंच या अँगरेज़ी गीत। कोई लोकप्रिय धुन और धीरे-धीरे दूसरी आवाज़ें पहली आवाज़ के संग मिलने लगतीं। या कभी ‘इण्टरनेशनल बिग्रेड’ का कोई प्रयाण-गीत जो मुद्दत पहले स्पेनिश गृह-युद्ध के जमाने में गाया जाता था या ‘टॉम ब्राउन्स बॉडी लाइज़ ए मोल्डरिंग इन द ग्रेव’-या फिर अवान्ती पोपोली जिसे गाते समय समूचा जहाज़ गूँजने लगता या कभी-कभी बहुत पुराना जहाज़ियों का गीत जो हमें हमेशा उदास कर देता-‘माई बौनी इज़ ओवर द ओशन, माई बौनी इज़ ओवर द सी-ब्रिंग बैक, ओ ब्रिंग बैक माई बौनी टु मी’...(मेरा यार सागर में है, मेरा यार समुद्र में है-बुला दो, ओ मेरे यार को बुला दो..)
ऐसी ही एक रात थी जब बर्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था, तो वह डेक पर राधाकृष्णन् की पुस्तक ‘हिन्दू व्यू ऑव लाइफ़’ पढ़ रही थी। मैंने उसे कभी अपने केबिन में जाते नहीं देखा था। मुझे लगता है कि वह रात के समय भी डेक पर सोती थी। वह पैसिफ़िस्ट संस्था की ओर से आइसलैंड जा रही थी। उसे यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ था कि मैं प्राग से आ रहा हूँ, ‘‘क्या यह कम्युनिस्ट देश नहीं है ?’’ उसने मुझसे सिगरेट माँगी दियासलाई जलाते समय मैंने क्षण-भर के लिए उसके गम्भीर चेहरे को देखा था।
कुछ देर तक हम चुपचाप सिगरेट पीते रहे।
‘‘कितने अरसे से आप पैसिफ़िस्ट संस्था में काम कर रही हैं ?’’
‘‘दो साल पहले घर छोड़ा था...तब से वापस नहीं गयी।’’
‘‘आपको यह काम भाता है ?’’
एक क्षण तक वह चुप रही।
‘‘मैंने कभी नहीं सोचा...इस प्रश्न के बारे में। जो भी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, करती हूँ। फिर भी बहुत कम...उसने बहुत कम जितनी ज़रूरत है, जितना कर सकती हूँ।’’
डेक लगभग ख़ाली हो गया है...ऊपर फ़र्स्ट क्लास के किसी केबिन में ग्रामोफ़ोन पर कोई रिकॉर्ड बजा रहा है-कभी-कभी लहरों के बीच इक्के-दुक्के सोते हुए यात्रियों की साँस सुनाई दे जाती है।
‘‘काफी लम्बा अरसा है-दो वर्ष।’’
‘‘ज़्यादा लम्बा नहीं, यदि उम्र लम्बी हो’’, उसने हँसते हुए कहा, ‘‘लेकिन मुझे कभी अपने निर्णय पर खेद नहीं हुआ। दो साल पहले मैं कुछ भी नहीं समझती थी। महज़ दिन-रात एक फ़िजूल सी बेचैनी महसूस करती थी और अब..वह क्षण भर रुकी मानो शब्दों को टटोल रही हो, ‘‘और अब कभी-कभी लगता है, जैसे मैं अपनी तरफ़ से ज़िन्दगी को मानी दे सकी हूँ...’’
‘‘अपनी तरफ़ से ?’’
‘‘हाँ, क्योंकि सूक्ष्म अर्थ में मुझे अपने काम से ज़्यादा सुकून नहीं मिलता।’’ उसकी आवाज़ हलके से सिहर गयी।
‘‘पिछले साल मैं अल्जीरिया गई थी-सिर्फ़ चन्द हफ़्तों के लिए। गाँव के गाँव तबाह हो गए हैं वहाँ...हज़ारों आदमी बिना घर-बार के, सड़कों पर भूखे और बीमार बच्चे। ‘मानव-उत्पीड़न’-पहली बार मुझे इस शब्द के सही मानी पता चले...उससे पहले मैं सिर्फ़ अख़बारों में पढ़ती थी, अल्जीरियायी शरणार्थियों के बारे में। तुमने भी पढ़ा होगा...लेकिन जब तक हम आँखों से नहीं देखते, कभी नहीं जानते...इतना भयानक !’’
कित्ता पानी ? कित्ता ? हाथ फैल जाते हैं, और नन्हें से आलिंग्न में समूचा अन्तहीन समुद्र सिमट आता है। मुद्दत पहले घर की छत पर मछलियों का खेल खेलते हुए क्या कभी सोचा था कि एक दिन सचमुच लहरें हमारे सिर पर से गुज़र जाएँगी और हम, जो अब बड़े हो गए हैं, बच्चों से डरते, ठिठुरते हुए डेक पर बैठे रहेंगे ?
या लेटे रहेंगे, कम्बलों में सिकुड़े हुए बंडलों-से-लंच की घंटी बजेगी तो भी, ‘डिनर’ की पुकार होगी तो भी ! बिना हिले-डुले, भूखे-प्यासे तपस्वियों से, अधसोए, अधजागे...
रात और दिन..
दो दिन तक समुद्र-पक्षी बराबर हमारे जहाज़ के पीछे उड़ते रहे, धूप और आँधी में, दिन-रात। जब जहाज़ के ‘किचन’ से बावर्ची पुरानी बासी रोटी के टुकड़े, फलों के छिलके या बची-खुची गोश्त की तरकारी बाहर फेंकता, तो वे उन पर उतावले-से होकर टूट पड़ते, समुद्र में गोते लगाते हुए उन्हें निगल लेते और फिर उड़ने लगते, उस घड़ी की आशा में जब बारह या तेरह घंटे बाद बावर्ची फिर अपना सिर ‘किचन’ की खिड़की से बाहर निकालेगा।
किसने कहा था कभी समुद्र-पक्षी के ‘रोमैंटिक’ सौन्दर्य के बारे में ? छह दिन का सागर-पथ है। कोपनहेगन से आइसलैंड तक। हर दिन को गिनना पड़ता है, समय का हिसाब रखने के लिए। और समय है जिसने अपने को दिन और रात के पहियों से मुक्त करके फैला दिया है, समुद्र की अबाध नीलिमा पर। लम्बे होते हुए दिन, सफ़ेद रातों-तले चीख़ती लहरें, पानी के बीच धरती पाने की बिलखती प्यास...
उदासी, चक्कर, थकान, इन सबसे मुठभेड़ बाद में हुई। पहले दिन सबके चेहरे पर ताज़गी, उल्लास और ललक, भोजन के प्रति उत्साह आधे पढ़े हुए उपन्यासों को ख़त्म करने की उमंग, नए मित्र बनाने का जोश-सबकुछ था। डेक की कुरसियाँ भरी रहतीं लड़कियों के बालों पर बँधे लाल, नीले हरे स्कार्फ़ हवा में उड़ते रहते, जहाज़ के कामों में प्रमियों के जोड़े समुद्र पर तिरते हुए सपनों में खोए रहते। जब कभी मौसम अच्छा होता, सब अपने-अपने कम्बलों में लिपटे हुए धूप सेंकने बैठे जाते। विभिन्न देशों के यात्री वहाँ जमा थे-स्विस, जर्मन स्वीड, डेन और अकेला एक भारतीय ! डेक के ऊपर ‘बार’ थी, फर्स्ट क्लास के सामने। अकसर रात्रि के भोजन के बाद जब डेक पर हवा तेज़ हो जाती और कम्बलों के बावजूद दाँत कटकटाने लगते, यात्रियों के छोटे-छोटे गुच्छे ‘बार’ में जा बैठते। बन्द खिड़कियों के परे समुद्र की अधीर, बेचैन चीखडें गूँजती रहतीं, मानो किसी बनैले जन्तु के पिंजड़े में बन्द कर दिया हो और वह हाँफता, बदहवास-सा होकर बाहर निकल आने के लिए छटपटा रहा हो ! चिड़ियाघर में बन्द क्या कभी सिंह को देखा है, उसकी क्षुब्ध, असहाय विक्षिप्त घुटन को ?
किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लमहों के लिए डेनिश बीयर या फ्रेंच कोन्याक पीते हुए हम भूल जाते कि हम असीम अँधेरे के एक छोटे-से टुकड़े पर तिर रहे हैं, कि हमारे नीचे एक नीली, रहस्यमय जादुई दुनिया बसी है, हमारे संग-संग रेंग रही है-क्षुब्ध, अशान्त और निस्तब्ध। इस दुनिया का आभास उसी समय होता जब कोई अल्लहड़ सी लहर पूरी निर्ममता से हमारे जहाज़ को धकेल देती और अचानक हमारे सामने मेज़ पर रखा बीयर का गिलास लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ता, और ‘बार’ में हर मेज़ पर अपने-अपने गिलासों को बचाने की बचकानी-सी भगदड़ मच जाती।
किन्तु समुद्र का यह नशा और उल्लास ज्यादा दिनों तक नहीं टिका रह सका। उत्तरी सागर के खुले, नग्न विस्तार में पहुँचते ही हमारे जहाज़ को अचानक प्रगैतिहासिक काल की बनैली, आदिम लहरों ने लपेट लिया। जान पड़ता था जैसे कोई अदृश्य दानव हमारे ‘गुलफॉस’ को एक नन्हें-से खिलौने की मानिन्द ऊपर-नीचे उछाल रहा हो ! डेक पर दो क़दम चलते हुए लगता था, जैसे हम एक छोटे से भूकम्प के भीतर से गुजर रहे हैं। जहाज़ अब ऊपर-नीचे न डोलता हुआ दाएँ-बाएँ हिचकोले खा रहा था। डेक पर पानी के चहबच्चे लग जाते थे और अब वहाँ बैठना ख़तरे से खाली नहीं था। जहाज के बीचोंबीच एक चौड़ा-सा चबूतरा था जो अपेक्षाकृत अधिक सूखा और सुरक्षित रहता था। डेक से खदेड़े जाने के बाद हमने बचाव का दूसरा मोर्चा यहीं पर गाड़ लिया था।
इस बीच कई परिचित मित्रों से धीरे-धीरे साथ छूटता गया। पहले दिन के जाने-पहचाने साथी अब बहुत कम डेक या भोजन-कक्ष में दिखाई देते थे और हम मन-ही-मन अनुमान लगा लेते थे कि वे ‘मृत्यु-शैया’ (मज़ाक में हमने ‘सी-सिकनेस’ को मृत्यु शैया की संज्ञा दे रखी थी) के शिकार हो गए हैं। ऐसा भी होता था कि किसी शाम ‘बार’ में हम किसी हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति से हँस-खुलकर गपशप कर रहे होते और दूसरे दिन वह सज्जन ऐसे ग़ायब हो जाते कि अगले चौबीस घंटों तक उनके दर्शन ही न होते। दोबारा मिलने पर उनका पीला, जर्द़ चेहरा देखते ही हम भाँप जाते कि वह बेचारे ‘तहख़ाने’ से वापस लौटे हैं।
तहख़ाना....यह नाम हमने अपने सेकेण्ड क्लास के सामूहिक केबिन को दे रखा था। हमारे लिए अलग-अलग केबिन नहीं थे, सब मिलजुलकर एक संग बैरकनुमा कमरे में सोते थे। एक बिस्तर के ऊपर दूसरा बिस्तर लगा था, बीच में सब लोगों का सामान और ईर्द-गिर्द बहुत ही मद्धिम बत्तियाँ, जैसे ‘फ़ाइटिंग-लाइन’ के पीछे कोई छोटा-सा अस्पताल हो ! इस अँधेरे, लम्बे सीलन-भरे ‘तहख़ाने’ में घुसते ही सिर चकराने लगता था-इससे छुटकारा पाने के लिए ही हम रात-दिन डेक पर डटे रहते थे, जिसे हमने ‘फ़ाइटिंग-लाइन’ का नाम दे रखा था।
लीथ की बन्दरगाह पहुँचने से पहले जहाज़ के यात्री खुद-ब-खुद तीन वर्गों में बँट चुके थे :
1. वे यात्री जिनके लिए समुद्र का होना-न-होना बराबर था। वे अकसर आराम से अपने-अपने बिस्तरों पर सोते रहते और जब ऊब जाते तो ‘बार’ में बैठकर बीयर पीते, आइलैंड का नक्शा देखते या ‘राइटिंग-टेबल’ पर चिट्ठियाँ लिखते। वे सुबह शाम यथासमय (या समय से पहले ही) ‘लंच’ और ‘डिनर’ लेने ‘डाइनिंग रूम’ जाते थे और मुस्कराते हुए तुष्ट भाव से वापस लौटते थे। हम सब उन्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे-इसके अलावा शायद हम कुछ कर भी नहीं सकते थे।
2. डेकवासी, जो चारों ओर शत्रुओं से घिरे थे। केबिन में जाते ही जिनका सिर चकराने लगता था, भोजन-कक्ष में भोजन को देखते ही मितली आने लगती थी और ‘बार’ में बैठकर मद्य-पदार्थों के सेवन के प्रति जिनके मन में गहरी सात्त्विक निरासक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। मृत्यु शैया से अपने को मुक्त रखने के लिए जिन्होंने डेक का सहारा पकड़ रखा था। रात-दिन कड़कड़ाती सरदी में ठिठुरते अपने-अपने स्लीपिंग बैग या कम्बलों में साँस लेती गठरियों से डेक के चबूतरे पर पड़े रहते थे-‘डिफ़ेन्स-लाइन’ के सिपाही। मैं इसी मण्डली के संग आख़िर तक घिसटता रहा।
3. और अन्त में मृत्यु-शैयावासी, जो डेक के कष्टों से घबराकर अपने गरम बिस्तरों पर लेटने का मोह सँवरण न कर सके और फिर वहीं के हो रहे। तहख़ाने के बिस्तरों पर उन्हें लेटे देखकर अकसर युद्ध में घायल सैनिकों का स्मरण हो आता, जो डेक की ‘डिफ़ेन्स-लाइन’ पर क्षत-विक्षत होने के कारण जहाज़ के डॉक्टर द्वारा यहाँ भेज दिए गए हों।
तीसरे दिन सुबह बदली और कुहरे के परदे पर ज़मीन की धुँधली-सी रूपरेखा दृष्टिगोचर हुई और गो हम बहुत पस्त और थके थे, लीथ बन्दरगाह का नाम सुनते ही डूबे और टूटे हौसलों को वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमारे जहाज़ को यहाँ पाँच-सात घंटे विश्राम लेना था और इस दौरान कोई भी जहाज़ पर रहने के लिए उत्सुक नहीं था। कुछ घड़ियों के लिए हम अँधेरे तहख़ाने, डेक की सरदी और जहाज़-सम्बन्धी हर चीज से छुटकारा पाने के लिए उतावले से हो उठे थे।
ज़मीन, दुकानें लोगों की परिचित आवाज़ें और पुराने गिरजे-लगा, जैसे हम एक लम्बी मुद्दत के बाद सभ्यता की दुनिया में वापस लौट आए हैं। यद्यपि हम जहाज़ से उतरकर ठोस धरती पर चलने लगे थे, हमें देर तक यही महसूस होता रहा जैसे हम शराबियों की मानिन्द किसी डोलती, डगमगाती चीज़ पर चल रहे हों। समुद्र अब भी हमारे संग था।
मन में पहले से यह भ्रम था-हालाँकि इस भ्रम का कोई विशेष आधार रहा हो, याद नहीं आता-कि बन्दरगाह से एडिनबोरो जाने में काफी देर लगेगी, किन्तु जब बस ने सिर्फ आधा घंटे में हमें शहर के बीचोबीच लाकर छोड़ दिया तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ और कुछ-कुछ निराशा भी। सबसे पहले चाय पी, चाय और टोस्ट-और तब पहली बार पूरी वास्तविकता से एहसास हुआ कि हम इंग्लैंड में हैं....इंग्लैंड न सही, स्कॉटलैंड में, किन्तु हर चीज़ बार-बार लन्दन के बीते दिनों का स्मरण करा जाती थी। डबलडेकर लाल बसें, एल और ड्राफ्ट के बीयर-घर, घरों के दरवाजे के सामने रखी दूध की बोतलें, ‘गार्डियन’ और ‘टाइम्स’ ‘प्लेयर्स प्लीज’ के विज्ञापन, हैम्बर्गर और हॉट डॉग और पेलीकन सीरीज़ की पुस्तकें, जिन्हें देखे अरसा गुज़र चुका था....
और कुहरा !
किन्तु रफ़्ता-रफ़्ता कुहरा उठने लगा था और हम खुलती, फीकी धूप की हलकी खुमारी में भीड़ के संग-संग घिसटते जा रहे थे। पहली बार पूरी शिद्दत से महसूस हुआ कि धरती, महज ठोस धरती पर चलने का भी अपना अलग सुख है। वह पैरों के नीचे काँपेगी नहीं, हिले डुलेगी नहीं, यह ख़याल मन को अजीब सान्त्वना-सी देता है। यदि हमें उस समय कोई यह कहता कि हम जिन्दगी-भर धरती पर ही चलते रहे थे तो हमें कुछ वैसा ही विस्मय होता जैसा मोलियर के ‘जैण्टिलमैन’ को यह जानकर हुआ था कि वह जीवन-भर गद्य में बातचीत करता रहा है।
ऊँचा-नीचा शहर एडिनबोरो, प्रिन्सेज़ स्ट्रीट पर चलते हुए आम स्कॉटिश लोग, पहाड़ी लोगों-से सहज और खुशमिज़ाज। लगता है, अँगरेज़ों की अभिजात औपचारिकता इन्हें नहीं छू गई है। सड़क के बीचोबीच ठठाकर हँसते हैं और अचानक याद हो आती है रॉबर्ट बर्न्स की। प्रिन्सेज़ स्ट्रीट के सामने ही एक छोटे-से बाग़ में बर्न्स का स्मारक है और उनकी मूर्ति के सामने स्मरण हो आते हैं मुद्दत पहले पढ़े उनके गीत, उनकी कविताएँ। कितना-कुछ जो हम स्कॉट जाति के बारे में जानते-बूझते हैं : जीने और मरने की भूखी हठीली चाह, हर अन्याय के विरुद्ध सुलगता विद्रोह, एक खुरदरी उच्छृंखल-सी अराजकता, गरीबी और गर्व, दूर पहाड़ियों की पुकार और शहरी पबों की पियक्कड़ चीखें-यह सब, और इसके अलावा बहुत-कुछ भी बर्न्स के गीतों से निकलकर हमारे संग-संग चलता है, एडिनबोरो की गलियों में।
शायद यह है-और ऐसा मैं सोचता हूँ, कि हमयात्री किसी भी जगह पहली बार नहीं जाते; हम सिर्फ लौट-लौट आते हैं उन्हीं स्थानों को फिर से देखने के लिए, जिसे कभी, किसी अनजाने क्षण में हमने अपने घर के कमरे में खोज लिया था। क्या यह कभी सम्भव कि हम ओसलो में घूमते रहें और अचानक गली के नुक्कड़ पर इब्सन के किसी पात्र से भेंट न हो जाए ! या पहली बार आइफल-टॉवर के सामने फैली पेरिस की छतों को देखकर हमें ‘अपने’ पेरिस की याद न हो आए जिसे हमने बाल्ज़क के उपन्यासों और रजिस्ताँ की कविताओं से चुराकर ख़ास अपनी निजी अल्बम में चिपका लिया था।
ये ख़याल बादलों की तरह बह आते हैं, स्कॉटमेमोरियल की पहाड़ी पर, जिसकी ढलान पर हम लेटे हैं। थोर्गियेर ने कुछ फोटो लिए हैं। हलकी-हलकी रुई में भरी आवाज़ें। सामने फैला है एडिनबोरो और उसके परे मेघाच्छन्न आकाश। फ़ोर्ट की ऊँची बुर्जियों पर परिन्दों का झुण्ड उड़ा जाता है। नीचे खड़े हैं बुझी-बुझी मैली धूप में शहर के मकान, कोयले और गर्द में सनी नंगी दीवारें, ऊँची-नीची छतें, चिमनियाँ, बरामदों में सूखते, हवा में फड़फड़ाते कपड़े। शहर वही है किन्तु पहाड़ी की चोटी से देखने पर बिलकुल बदल गया है, जैसे हम उसकी फ़ोटो का ‘नेगेटिव’ देख रहे हों !
किन्तु आँखें शहर की चिमनियों के परे फिसल जाती हैं-उस ओर जहाँ धरती का आँचल भीग रहा है नीली स्याही में। एक गीला बैंगनी रंग, फीकी, धूप में घुलता, फैलता। उत्तर की ओर जहाँ एक अदृश्य बिन्दु पर आइसलैंड टिका है-नीली चट्टानें जहाँ मोम-सी बनकर धूप में पिघल रही हैं और बादल हैं, जो थिएटर के परदों से हवा में टँगे हैं, जिन्हें हमारा जहाज़ एक-एक करके उठाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा।
हम धूप में ऊँघने लगे हैं। हवा चलती है और अजीब कोमल-सी सरसराहट होती है कानों के पास। घास तितलियाँ या महज़ हवा। थोर्गियेर दूरबीन से बन्दरगाह की ओर देख रहे हैं। सोते हुए भी मुझे लहरों का स्वर सुनाई देता है...जैसे कोई रो रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं है-सिर्फ़ हवा में सरसराती घास है और ऊपर बादल हैं और समुद्र बहुत दूर है...अचानक थोर्गियार मेरा कन्धा हिलाते हैं, ‘‘देखो...उस तरफ़’’,-वह उँगली से इशारा करते हैं और दूरबीन मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं। एक नन्हा-सा सफ़ेद धब्बा दूरबीन के शीशे पर सिमट आया है-गुलफ़ॉस ! हमारा जहाज़। दूर से वह कितना अरक्षित और असहाय-सा दिखाई देता है !
‘‘अब हमें चलना चाहिए’’, थोर्गियेर ने जम्हाई लेते हुए कहा। सोने की जबरदस्त इच्छा होती है, घास पर भूल जाने की इच्छा होती है कि हमें फिर डेक की ‘डिफेन्स-लाइन’ में जाना होगा लेकिन हम नीचे उतरते जाते हैं, दोपहर की लम्बी छायाओं के संग...बीच यात्रा में मुहब्बत से बचना चाहिए,’’ एक पुरानी चीनी कविता की पंक्ति याद आती है।
समय कम और सीमित है। शाम को चार बजे तक जहाज़ पर पहुँच जाना होगा-इतना समय नहीं कि जहाज़ पर भोजन करने के बाद वापस शहर लौटा जा सके। हम चाय पीकर ही सन्तुष्ट हो गए हैं। ‘फ़ोर्ट’ और ‘आर्ट गैलरी’ के बीच चुनाव करना ही होगा, दोनों को देखने का समय नहीं है। निर्णय करने में ज्यादा ऊहापोह नहीं करनी पड़ी। हमारे पाँव एडिनबोरो आर्ट गैलरी के चौड़े दरवाज़ो की तरफ बढ़ जाते हैं।
कितने कम याद रह पाते हैं चित्र, दीवार पर टँगे फ्रेमों में बन्द खून और पसीने में लिथड़े स्वप्न ! और हम हैं कि हर कदम पर सदियों को पार करते जातें हैं। संग रह जाता है केवल एक आभास-रंगों और आकृतियों से उत्पन्न हुई किन्तु उससे अलग एक स्मृति। शून्यता को काटती एक उड़ान, एक चीख़। बन्द सदियों की कुछ चाभियाँ, जिन्हें हम अपने संग ले आते हैं और बाद में खोलते हैं; अकेले में, अपने ही अकेलेपन को।
जब कभी एडिनबोरो की ‘आर्ट गैलरी’ के बारे में सोचता हूँ आँखों के सामने घूम जाते हैं तितियान के चित्र...लगता है, जैसे मानव-आत्मा अपने सब बन्धनों को तोड़कर सुनहरे असीम आलोक के ज्वलन्त रंगों में फैल गई है। तितियान के देवदूत असीम दूरियाँ लाँघते हुए एक ऐसे मांसल आनन्द को खींच लाते हैं जिसमें रहस्यमय अथवा अशरीरी कुछ भी नहीं है, धरती के ऊपर उड़ते हुए भी जो धरती की गन्ध और आत्मीयता को नहीं छोड़ पाते और बरबस मुझे बैरन्सन के शब्द याद हो आते हैं : ‘पुनर्जागर की सच्ची पवित्र सन्तानें, जिन्दगी के भय और ओछेपन से सर्वथा मुक्त।’ गैलरी में मेरे प्रिय चित्रकारों-रैम्ब्राँ हालास और स्टील के भी चित्र हैं, किन्तु इतने कम कि भूख नहीं मिटा पाते। सिर्फ़ एक एलग्रेको। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे उस समय हुआ जब अचानक गैलरी के एक अलग छोटे-से कक्ष में सिर्फ़ पूसाँ के चित्र दिखाई दिए-‘सेवेन सेक्रामेंट्स’ का पूरा सेट। नि:सन्देह कोई भी गैलरी फ्रेंच कलाकार की इन अद्वितीय अमर कृतियों पर गर्व कर सकती है। दीवार के एक कोने में बैलिनी के वे उद्गार उद्घृत किए गए हैं जो उन्होंने ‘सेवन सेक्रामेंट्स’ को पहले-पहल देखकर प्रकट किए थे। काश, मैं उन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख पाता।
उस रात पहली बार जहाज़ के विभिन्न वर्ग आपस में घुल मिल गए और हम देर तक ‘बार’ में बैठकर बीयर पीते रहे...बिना किसी डर या आशंका के-मानो हम प्राग के ही किसी ‘पब’ में बैठे हों। समुद्र पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक स्थिर था, किन्तु यह स्थिरता ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, यह हम जानते थे। शायद इसी कारण अनेक यात्री ‘मृत्यु-शैया’ पर जाने से पहले मुक्ति के इन चन्द लमहों को खुले और अकुण्ठित मन से जी लेना चाहते थे।
लीथ छोड़ने के बाद डेक पर अनेक चेहरे दिखाई देने लगे हैं। इंग्लैंड से अनेक नए यात्री जहाज़ पर आए हैं, केवल अँगरेज़ ही नहीं, विभिन्न देशों के लोग। ‘बार’ की मेज पर दो स्विस लड़कियों से परिचय हुआ। उन्हें केवल यह चिन्ता सता रही थी कि आइसलैंड में अच्छा दूध मिलेगा या नहीं, ‘‘दूध नहीं मिला, तो ज्यादा दिन मैं नहीं रह सकूँगी।’’
‘‘दूध के बारे में मुझे नहीं मालूम लेकिन दुर्भाग्यवश बीयर पर पाबन्दी है,’’ मैंने कहा।
बीयर से उन्हें ख़ास लगाव नहीं था, अतः इस समाचार से उन्हें कोई विशेष दुख नहीं हुआ। बाद में पता चला उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है (‘क्या हमसे ज्यादा खराब ?’ मैंने मन-ही-मन सोचा) और वे ‘हिचहाइकिंग’ द्वारा ही आइसलैंड का भ्रमण करेंगी। उस रात के बाद हमने उन्हें आइसलैंड पहुँचने तक नहीं देखा..टॉमस मान के सेनेटोरियम के मरीज़ों की भाँति इस जहाज़ पर जाने-पहचाने लोग अचानक ग़ायब हो जाते हैं और फिर उनके बारे में बातचीत करना ‘बैड-टेस्ट’ माना जाता है।
लीथ की बन्दरगाह से पुरातत्त्वशास्त्र और भूगर्भशास्त्र के अनेक अँगरेज़ छात्र-छात्राएँ जहाज़ पर दिखाई देते हैं। उनका अपना एक अलग झुण्ड है और वे हमेशा एक संग घूमते हैं। किन्तु हमारे सबसे आत्मीय और दिलचस्प मित्र कुछ ‘पेसिफ़िस्ट’ युवक-युवतियाँ हैं जो आइसलैंड में लूले-लँगड़े बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने बातचीत करते हुए मुझे बताया कि यद्यपि वे एक ही संस्था के सदस्य हैं, उनमें से हर व्यक्ति को हर समस्या पर अपने स्वाधीन विचार रखने का अधिकार है। उनमें से कुछ लोग आणविक-निःशस्त्रीकरण कमेटी (अध्यक्ष : बर्ट्रेण्ड रसेल) के समर्थक हैं। एक बुद्धिजीवी से दिखनेवाले युवक ने जिनकी लम्बी ऊबड़-खाबड़ दाढ़ी है और जो हमेशा नीली जीन्स पहने रहते हैं जिनकी जेबों में किताबें भरी रहती हैं..‘बीटनिक कवि ?’ मैं सोचता हूँ), मुझे देखते ही तपाक से हाथ मिलाया है, ‘‘मैंने आपको कहीं देखा है-आप एल्डर मास्टन-मार्च में तो नहीं थे ?’’
‘‘नहीं, उन दिनों मैं इंग्लैंड में नहीं था-लेकिन शायद आपने मुझे ट्रिफ़ाल्गर स्क्वॉयर में देखा होगा, कभी-कभी मैं वहाँ जाया करता था।’’ काफ़ी देर तक हम लन्दन के बारे में बातचीत करते रहे। वह भी मेरी ही तरह ‘डेकवासी’ थे। अकसर बहसों के दौरान (वह एकतरफा नि:शस्त्रीकरण के समर्थक थे) मैं चुपचाप उनके तर्क सुना करता था।
बीच के इन दिनों में देर रात तक डेक पर लम्बी और कभी-कभी उत्तेजनापूर्ण बहसें हुआ करती थीं...लगभग सभी ‘डेक-वासी’ इनमें भाग लेते थे। एकतरफ़ा निःशस्त्रीकरण (जो सबसे ज्यादा ‘जलता प्रश्न’ था) से लेकर आइख़मैन के मुक़दमे तक...न प्रश्नों की कमी थी, न समय का अभाव। हमें काफ़ी ऊँचे स्वर में बोलना पड़ता था ताकि हमारी आवाज़ लहरों से ऊपर उठ सके।
हमारा जहाज़ अटलाण्टिक सागर के बीच आ चुका था। जितना ही अधिक वह उत्तर की ओर सरकता जाता था, रातें ज्यादा सफ़ेद होती जाती थीं। एक असीम उजाला। रात और दिन की सीमा-रेखा दिन-पर-दिन धुँधली होती जा रही थी। अकसर हम आधी रात तक अपने-अपने स्लीपिंग बेड में लिपटे डेक पर लेटे रहा करते थे। ‘बार’ की बत्ती बुझ जाती थी, फ़र्स्ट क्लास के केबिन अँधेरे में डूब जाते थे और चारों ओर एक घना, गहरा सन्नाटा घिर आता था-सिर्फ़ लहरें थीं जो कभी चुप नहीं होती थीं किन्तु अब हम उनकी ओर से निरासक्त हो चले थे। हम लेटे रहते, और धीरे-धीरे तारों से आकाश भरने लगता। जुलाई का नीरव उजला आकाश। आकाश और बहुत पुराना अतीत। हर एक की अलग स्मृतियाँ। और हम डेक पर लेटे हुए एक दूसरे की साँस सुनते रहते....नींद नहीं आती थी। तब अचानक कोई धीमे, बहुत धीमे स्वर में गाने लगता था। कोई जर्मन फ़ेंच या अँगरेज़ी गीत। कोई लोकप्रिय धुन और धीरे-धीरे दूसरी आवाज़ें पहली आवाज़ के संग मिलने लगतीं। या कभी ‘इण्टरनेशनल बिग्रेड’ का कोई प्रयाण-गीत जो मुद्दत पहले स्पेनिश गृह-युद्ध के जमाने में गाया जाता था या ‘टॉम ब्राउन्स बॉडी लाइज़ ए मोल्डरिंग इन द ग्रेव’-या फिर अवान्ती पोपोली जिसे गाते समय समूचा जहाज़ गूँजने लगता या कभी-कभी बहुत पुराना जहाज़ियों का गीत जो हमें हमेशा उदास कर देता-‘माई बौनी इज़ ओवर द ओशन, माई बौनी इज़ ओवर द सी-ब्रिंग बैक, ओ ब्रिंग बैक माई बौनी टु मी’...(मेरा यार सागर में है, मेरा यार समुद्र में है-बुला दो, ओ मेरे यार को बुला दो..)
ऐसी ही एक रात थी जब बर्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था, तो वह डेक पर राधाकृष्णन् की पुस्तक ‘हिन्दू व्यू ऑव लाइफ़’ पढ़ रही थी। मैंने उसे कभी अपने केबिन में जाते नहीं देखा था। मुझे लगता है कि वह रात के समय भी डेक पर सोती थी। वह पैसिफ़िस्ट संस्था की ओर से आइसलैंड जा रही थी। उसे यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ था कि मैं प्राग से आ रहा हूँ, ‘‘क्या यह कम्युनिस्ट देश नहीं है ?’’ उसने मुझसे सिगरेट माँगी दियासलाई जलाते समय मैंने क्षण-भर के लिए उसके गम्भीर चेहरे को देखा था।
कुछ देर तक हम चुपचाप सिगरेट पीते रहे।
‘‘कितने अरसे से आप पैसिफ़िस्ट संस्था में काम कर रही हैं ?’’
‘‘दो साल पहले घर छोड़ा था...तब से वापस नहीं गयी।’’
‘‘आपको यह काम भाता है ?’’
एक क्षण तक वह चुप रही।
‘‘मैंने कभी नहीं सोचा...इस प्रश्न के बारे में। जो भी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, करती हूँ। फिर भी बहुत कम...उसने बहुत कम जितनी ज़रूरत है, जितना कर सकती हूँ।’’
डेक लगभग ख़ाली हो गया है...ऊपर फ़र्स्ट क्लास के किसी केबिन में ग्रामोफ़ोन पर कोई रिकॉर्ड बजा रहा है-कभी-कभी लहरों के बीच इक्के-दुक्के सोते हुए यात्रियों की साँस सुनाई दे जाती है।
‘‘काफी लम्बा अरसा है-दो वर्ष।’’
‘‘ज़्यादा लम्बा नहीं, यदि उम्र लम्बी हो’’, उसने हँसते हुए कहा, ‘‘लेकिन मुझे कभी अपने निर्णय पर खेद नहीं हुआ। दो साल पहले मैं कुछ भी नहीं समझती थी। महज़ दिन-रात एक फ़िजूल सी बेचैनी महसूस करती थी और अब..वह क्षण भर रुकी मानो शब्दों को टटोल रही हो, ‘‘और अब कभी-कभी लगता है, जैसे मैं अपनी तरफ़ से ज़िन्दगी को मानी दे सकी हूँ...’’
‘‘अपनी तरफ़ से ?’’
‘‘हाँ, क्योंकि सूक्ष्म अर्थ में मुझे अपने काम से ज़्यादा सुकून नहीं मिलता।’’ उसकी आवाज़ हलके से सिहर गयी।
‘‘पिछले साल मैं अल्जीरिया गई थी-सिर्फ़ चन्द हफ़्तों के लिए। गाँव के गाँव तबाह हो गए हैं वहाँ...हज़ारों आदमी बिना घर-बार के, सड़कों पर भूखे और बीमार बच्चे। ‘मानव-उत्पीड़न’-पहली बार मुझे इस शब्द के सही मानी पता चले...उससे पहले मैं सिर्फ़ अख़बारों में पढ़ती थी, अल्जीरियायी शरणार्थियों के बारे में। तुमने भी पढ़ा होगा...लेकिन जब तक हम आँखों से नहीं देखते, कभी नहीं जानते...इतना भयानक !’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book